भारत-दुर्दशा (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)
नाभादास: जीवन परिचय और योगदान
जन्म और प्रारंभिक जीवन:
- नाभादास का जन्म 1570 ई. के आस-पास हुआ था।
- दक्षिण भारत में जन्म लेने के बाद, उनके पिता की मृत्यु हो गई और वे अपनी माता के साथ राजस्थान के जयपुर में आकर बसे। दुर्भाग्यवश, उनका अपनी माता से भी बिछोह हो गया।
- नाभादास का जीवन कठिनाईयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया।
शिक्षा और गुरुओं का प्रभाव:
- उन्होंने भगवद्भक्ति और काव्य रचना में गहरी रुचि दिखाई।
- उनके गुरु स्वामी अग्रदास थे, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे।
कृतियाँ:
- नाभादास की प्रमुख कृति “भक्तमाल” है, जो 1585-1596 के बीच लिखी गई थी। यह कृति भक्त चरित्रों का संग्रह है और इसे वैष्णव भक्ति का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है।
- अन्य कृतियों में “अष्टयाम” (ब्रजभाषा गद्य में) और “रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह” शामिल हैं।
विशेषताएँ:
- नाभादास का पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि दलित वर्ग की मानी जाती है।
- वे सगुणोपासक रामभक्त कवि थे, लेकिन उनकी भक्ति में माधुर्यभाव का पुट था।
- उनकी रचनाओं में वैष्णव भक्ति का गहरा प्रभाव है और वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे।
भक्तमाल की विशिष्टताएँ:
- “भक्तमाल” में नाभादास ने वैष्णव भक्तों के चरित को छप्पय छंद में वर्णित किया है।
- इस ग्रंथ में धर्म-संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेदकारी आग्रहों को महत्त्व न देते हुए केवल वैष्णवता को ही ध्यान में रखा गया है।
- यह ग्रंथ मध्ययुगीन हिंदी आलोचना का महत्वपूर्ण प्रमाण है और यह वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए अत्यधिक प्रामाणिक सामग्री प्रदान करता है।
उद्धरण और काव्य:
- “भक्तमाल” में नाभादास ने कबीर और सूरदास जैसे महान भक्त कवियों पर भी छंद लिखे हैं, जो उनके गहरे चिंतन और मनन का परिणाम हैं।
I) भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाए ।
योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए ||
हिंदू तुरक प्रमान प्रमान रमैनी सबदी साखी |
पक्षपात नहिं बचन सबहिके हितकी भाषी ।।
आरूढ़ दशा है जगत पै, मुख देखी नाहीं भनी ।
कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी ।
इस छंद में नाभादास ने संत कबीर की भक्ति और उनकी विचारधारा का वर्णन किया है। इसे सरल हिंदी में समझाने का प्रयास करते हैं:
शब्दार्थ और भावार्थ:
- भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाए: जो भी धर्म (धार्मिक क्रियाएँ) भक्ति से दूर हो, उसे कबीर ने अधर्म (गलत) मान लिया। यानी, धर्म का असली सार भक्ति में है। यदि धर्म में भक्ति नहीं है, तो वह अधर्म के समान है।
- योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए: कबीर के अनुसार, योग, यज्ञ, व्रत, दान आदि सभी कर्म (धार्मिक कार्य) यदि भजन (ईश्वर की उपासना) के बिना किए जाएं, तो वे निरर्थक हैं।
- हिंदू तुरक प्रमान प्रमान रमैनी सबदी साखी: कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से देखा। उन्होंने अपने दोहे (रमैनी), सबद (भजन) और साखियों के माध्यम से किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। उनके विचार सभी के लिए समान थे।
- पक्षपात नहिं बचन सबहिके हितकी भाषी: कबीर का कोई भी वचन पक्षपातपूर्ण नहीं था, वे हमेशा सभी के हित की बात करते थे।
- आरूढ़ दशा है जगत पै, मुख देखी नाहीं भनी: कबीर ने देखा कि संसार में सभी बाहरी दिखावे (मुख देखने) पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन असली सत्य को नहीं समझते।
- कबीर कानि राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी: कबीर ने किसी भी वर्ण (जाति) या आश्रम (जीवन के चार आश्रम) की परंपराओं का पालन नहीं किया। वे समाज में प्रचलित धार्मिक सिद्धांतों (षटदर्शन) से बंधे नहीं थे।
सारांश: इस छंद में नाभादास ने बताया है कि कबीर ने धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों की तुलना में भक्ति को अधिक महत्व दिया। उनके विचारों में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं था, और वे सभी के लिए समान रूप से भलाई की बात करते थे। कबीर बाहरी आडंबरों और समाज के नियमों से ऊपर उठकर, सच्ची भक्ति और ईश्वर के साक्षात्कार को प्राथमिकता देते थे।
II) उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अतिभारी ।
वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी ॥
प्रतिबिंबित दिवि दृष्टि हृदय हरि लीला भासी ।
जन्म कर्म गुन रूप सबहि रसना परकासी ॥
विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुन श्रवननि धरै ।
सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहिं शिरचालन करै ।
इस श्लोक में सूरदास की कविता की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। सरल हिंदी में इसका अर्थ इस प्रकार है:
- उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अतिभारी: सूरदास की रचनाओं में उक्ति (कहने की शैली), अनुप्रास (अलंकार), और वर्ण (शब्दों का चयन) अत्यंत प्रभावशाली और सटीक हैं।
- वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी: उनके वचनों में प्रेम और भावनाओं की अभिव्यक्ति इतनी गहरी होती है कि अर्थ भी अद्भुत और मनमोहक होते हैं।
- प्रतिबिंबित दिवि दृष्टि हृदय हरि लीला भासी: उनकी कविता में दिव्य दृष्टि (आध्यात्मिक दृष्टिकोण) प्रतिबिंबित होती है और हृदय में भगवान की लीला (क्रीड़ा) स्पष्ट रूप से झलकती है।
- जन्म कर्म गुन रूप सबहि रसना परकासी: उनकी कविताओं में भगवान के जन्म, कर्म, गुण और रूप का विस्तृत वर्णन होता है, जो सभी को आनंदित करता है।
- विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुन श्रवननि धरै: वह व्यक्ति बहुत ही शुद्ध बुद्धि का होता है, जो सूरदास के इन गुणों को सुनता और समझता है।
- सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहिं शिरचालन करै: सूरदास की कविताएं सुनकर ऐसा कौन सा कवि है, जो सिर न हिलाए (सम्मान और सराहना में)।
संक्षेप में, इस श्लोक में सूरदास की कविताओं की महानता और उनकी प्रभावशाली शैली की सराहना की गई है। उनकी कविताओं में भावनाओं, आध्यात्मिकता, और भगवान की लीलाओं का अद्भुत चित्रण होता है, जिसे सुनकर कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।
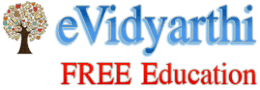
Leave a Reply