Notes For All Chapters – संस्कृत Class 8
सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते
(सही वर्णों के प्रयोग से (या शुद्ध उच्चारण द्वारा) व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है।)
१. पाठस्य परिचयः
- पाठः ‘सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते’ इति नाम्ना ‘हितोपदेशः’ इत्यस्मात् ग्रन्थात् स्वीकृतः।
- शुद्धं स्पष्टं च उच्चारणं व्याकरणस्य महत्त्वं च दर्शति।
- कथायां वृत्रासुर-इन्द्रयोः संनादति, यत्र स्वरपरिवर्तनेन अर्थभेदः संजातः।
हिन्दी अनुवाद
१. पाठ का परिचय
- पाठ का नाम ‘सम्यग्वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते’ है, जो ‘हितोपदेश’ ग्रंथ से लिया गया है।
- यह पाठ शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण तथा व्याकरण के अध्ययन के महत्व को दर्शाता है।
- कथा में वृत्रासुर और इन्द्र का प्रसंग है, जहाँ स्वर परिवर्तन से मंत्र का अर्थ बदल गया।
२. कथासारांशः
- इन्द्रः देवानां राजा, वृत्रासुरः असुराणां राजा।
- देवासुरयोः वैरभावः सर्वदा।
- वृत्रासुरः इन्द्रं जेतुं यज्ञं कारितवान्, मन्त्रः ‘इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व’।
- ऋत्विजः स्वरं परिवर्त्य अर्थं परिवर्तितवन्तः, येन इन्द्रस्य बलं वर्धितम्।
- बलवान् इन्द्रः वज्रेण वृत्रासुरं मारितवान्।
हिन्दी अनुवाद
२. कथा का सार
- इन्द्र देवताओं का राजा था, और वृत्रासुर असुरों का राजा था।
- दोनों के बीच सदा शत्रुता रहती थी।
- वृत्रासुर ने इन्द्र को हराने के लिए यज्ञ किया, जिसमें मंत्र था ‘इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व’।
- पुरोहितों ने स्वर बदलकर मंत्र का अर्थ बदला, जिससे इन्द्र का बल बढ़ गया।
- बलवान इन्द्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर को मार डाला।
३. शब्दार्थाः (मुख्यशब्दानां अर्थाः)
ऋत्विजः – पुरोहिताः (पुरोहित)
श्वजनः – शुनकः (कुत्ता)
सकम्: – सम्पूर्णम् (सम्पूर्ण)
शकलम्: – खण्डम् (टुकड़ा)
सकृत्: – एकवारम् (एक बार)
शकृत्: – विष्ठा (विष्ठा)
अव्यक्ताः – अस्पष्टाः (अस्पष्ट)
पीडिताः – अधिकप्रयत्नयुक्ताः (अत्यधिक प्रयासयुक्त)
महीयते: – सम्मानं प्राप्नोति (सम्मानित होता है)
व्याघ्री: – शार्दूला (बाघिन)
दंष्ट्राभ्याम्: – दन्ताभ्याम् (दाँतों से)
माधुर्यम्: – मधुरभावः (मधुरता)
अक्षरव्यक्तिः – अक्षराणां स्पष्टोच्चारणम् (अक्षरों की स्पष्टता)
सुस्वरः – शोभनः स्वरः (मधुर स्वर)
धैर्यम्: – विश्वासः (आत्मविश्वास)
शीघ्री: – वेगेन पठति (तेजी से पढ़ने वाला)
शिरःकम्पी: – शिरः कम्पति (सिर हिलाकर पढ़ने वाला)
अनर्थज्ञः – अर्थं न जानाति (अर्थ न जानने वाला)
अल्पकण्ठः – मन्दस्वरः (धीमे स्वर वाला)
४. श्लोकानां भावार्थः
श्लोक १:
पदच्छेदः यद्यपि बहु न अधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् स्वजनः श्वजनः मा अभूत् सकलम् शकलम् सकृत् शकृत्।
अन्वयः पुत्र! यद्यपि बहु न अधीषे तथापि व्याकरणं पठ। येन स्वजनः श्वजनः, सकलम् शकलम्, सकृत् शकृत् न भवेत्।
भावार्थः पुत्र! यद्यपि बहु न पठति, तथापि व्याकरणं पठ। येन स्वजनः (बन्धुः) श्वजनः (कुक्कुरः), सकलम् (पूर्णम्) शकलम् (खण्डम्), सकृत् (एकवारम्) शकृत् (विष्ठा) न भवति।
हिन्दी अनुवाद
श्लोक १:
पदच्छेद: यद्यपि बहु न अधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् स्वजनः श्वजनः मा अभूत् सकलम् शकलम् सकृत् शकृत्।
अन्वय: पुत्र! यद्यपि बहुत न पढ़े, तथापि व्याकरण पढ़। जिससे स्वजनः (बन्धु) श्वजनः (कुत्ता), सकलम् (पूर्ण) शकलम् (टुकड़ा), सकृत् (एक बार) शकृत् (विष्ठा) न हो।
भावार्थ: पुत्र! भले ही तुम बहुत कुछ न पढ़ सको, पर व्याकरण अवश्य पढ़ो। इससे उच्चारण में स्वजन (बन्धु) कुत्ता, सकल (पूर्ण) टुकड़ा, और एक बार विष्ठा न बन जाए।
श्लोक २:
पदच्छेदः व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्याम् न च पीडयेत् भीता पतनभेदाभ्याम् तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्।
अन्वयः यथा व्याघ्री पतनभेदाभ्यां भीता दंष्ट्राभ्यां पुत्रान् हरेत् न च पीडयेत्, तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्।
भावार्थः यथा व्याघ्री दन्तैः शिशुं न पीडति, न च पतति, तथैव वर्णान् नातिकठोरं नातिशैथिल्येन उच्चारति।
हिन्दी अनुवाद
श्लोक २:
पदच्छेद: व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्याम् न च पीडयेत् भीता पतनभेदाभ्याम् तद्वत् वर्णान् प्रयोजयेत्।
अन्वय: जैसे व्याघ्री पतन और भेद से डरकर दाँतों से शिशु को ले जाती है, पर पीड़ा नहीं देती, वैसे ही वर्णों का प्रयोग करें।
भावार्थ: जैसे बाघिन अपने शिशु को दाँतों से बिना चोट पहुँचाए ले जाती है, वैसे ही वर्णों का न अति कठोर और न अति शिथिल उच्चारण करना चाहिए।
श्लोक ३:
पदच्छेदः एवम् वर्णाः प्रयोक्तव्याः न अव्यक्ताः न च पीडिताः सम्यक् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते।
अन्वयः एवम् वर्णाः न अव्यक्ताः न च पीडिताः प्रयोक्तव्याः। सम्यक् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते।
भावार्थः वर्णाः स्पष्टं स्वाभाविकं च उच्चारणीयाः। सम्यक् उच्चारणेन समाजे सम्मानं प्राप्नोति।
हिन्दी अनुवाद
श्लोक ३:
पदच्छेद: एवम् वर्णाः प्रयोक्तव्याः न अव्यक्ताः न च पीडिताः सम्यक् वर्णप्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते।
अन्वय: इस प्रकार वर्ण न अस्पष्ट और न अति प्रयासयुक्त उच्चारित करें। सम्यक् वर्णप्रयोग से ब्रह्मलोक में सम्मान मिलता है।
भावार्थ: वर्णों को स्पष्ट और स्वाभाविक रूप से उच्चारित करना चाहिए। इससे समाज में सम्मान प्राप्त होता है।
श्लोक ४:
पदच्छेदः माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षट् एते पाठका गुणाः।
अन्वयः माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदः सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च एते षट् पाठकाः गुणाः।
भावार्थः मधुरं स्पष्टं उच्चारणम्, समुचितः पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यम्, तल्लीनता च उत्तमपाठकस्य गुणाः।
हिन्दी अनुवाद
श्लोक ४:
पदच्छेद: माधुर्यम् अक्षरव्यक्तिः पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षट् एते पाठका गुणाः।
अन्वय: माधुर्यम्, अक्षरव्यक्तिः, पदच्छेदः, सुस्वरः, धैर्यं, लयसमर्थं च ये छह पाठक के गुण हैं।
भावार्थ: मधुरता, अक्षरों की स्पष्टता, उचित पदच्छेद, मधुर स्वर, आत्मविश्वास और तल्लीनता उत्तम पाठक के छह गुण हैं।
श्लोक ५:
पदच्छेदः गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः अनर्थज्ञः अल्पकण्ठः च षट् एते पाठकाधमाः।
अन्वयः गीती शीघ्री शिरःकम्पी लिखितपाठकः अनर्थज्ञः अल्पकण्ठः च एते षट् पाठकाधमाः।
भावार्थः गीतवत्, शीघ्रं, शिरः कम्पति, लिखित्वा पठति, अर्थं न जानाति, मन्दस्वरः च अधमपाठकस्य दोषाः।
हिन्दी अनुवाद
पदच्छेद: गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः अनर्थज्ञः अल्पकण्ठः च षट् एते पाठकाधमाः।
अन्वय: गीती, शीघ्री, शिरःकम्पी, लिखितपाठकः, अनर्थज्ञः, अल्पकण्ठः च ये छह अधम पाठक हैं।
भावार्थ: गीत की तरह, तेजी से, सिर हिलाकर, लिखकर पढ़ने वाला, अर्थ न जानने वाला, और धीमे स्वर वाला अधम पाठक है।
पाठस्य प्रेरणा
- शुद्धं स्पष्टं च उच्चारणं व्याकरणाध्ययनं च आवश्यकम्।
- सम्यक् उच्चारणेन अर्थभेदः निवारति, सम्मानं च प्राप्यते।
- पाठकस्य गुणाः (माधुर्यम्, अक्षरव्यक्तिः इत्यादयः) वर्धनीयाः।
हिन्दी अनुवाद
पाठ की प्रेरणा
- शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण तथा व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है।
- सही उच्चारण से अर्थ का भेद टलता है और समाज में सम्मान मिलता है।
- पाठक के गुण जैसे मधुरता, स्पष्टता आदि को विकसित करना चाहिए।

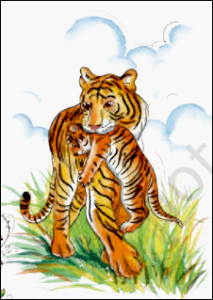
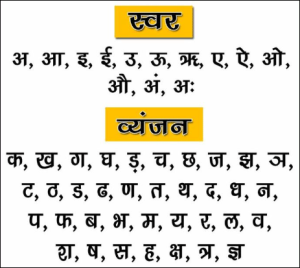

Leave a Reply