Notes For All Chapters – संस्कृत Class 8
वर्णोच्चारण-शिक्षा १
(अक्षरों का उच्चारण-अभ्यास १)
१. पाठस्य परिचयः
- पाठः ‘वर्णोच्चारण-शिक्षा १’ इति नाम्ना, शब्दानां सम्यक् शुद्धं च उच्चारणं महत्त्वपूर्णं दर्शयति।
- पूर्वपाठे वर्णानां उच्चारणं दृष्टवन्तः, अधुना प्रत्येकवर्णस्य शुद्धोच्चारणं ज्ञास्यामः।
- वर्णानां स्वर-व्यञ्जनादिभेदाः पूर्वकक्षासु ज्ञाताः।
- उच्चारणे आस्यं, नाभिप्रदेशः, उरः, कण्ठबिलः च उपयोगी भवन्ति।
हिन्दी अनुवाद
- पाठ का नाम ‘वर्णोच्चारण-शिक्षा १’ है, जो शब्दों के सम्यक् और शुद्ध उच्चारण के महत्व को दर्शाता है।
- पिछले पाठ में वर्णों के उच्चारण को देखा, अब प्रत्येक वर्ण के शुद्ध उच्चारण को जानेंगे।
- वर्णों के स्वर-व्यंजन आदि भेद पूर्व कक्षाओं में ज्ञात हैं।
- उच्चारण में मुँह, नाभि-प्रदेश, छाती, गले का बॉक्स आदि उपयोगी हैं।
२. वागुत्पत्तिप्रक्रिया (Voice Production Mechanism)
- वर्णोच्चारणार्थं शरीरस्य चत्वारि तन्त्राणि:
1. नाभिप्रदेशः (मांसपेशीबलतन्त्रम्) – मांसपेश्यः उरं नोदयन्ति।
2. उरः (वायुबलतन्त्रम्) – श्वासकोशस्थितं वायुम् ऊर्ध्वं निःसारयति।
3. कण्ठबिलः (ध्वनितन्त्रम्) – वायुः कण्ठबिलं प्राप्नोति।
4. आस्यं (उच्चारणतन्त्रम्) – वायुः आस्यं प्रविश्य मुखे/नासिकायां वर्णरूपेण प्रकटीभवति।
आस्याभ्यन्तरे: मुखं (ओरल् कैविटी), नासिका (नेजल् कैविटी)।
प्रक्रिया: नाभिप्रदेश → उरः → कण्ठबिल → आस्यं → स्थानेषु वर्णोत्पत्तिः।
हिन्दी अनुवाद
- वर्ण उच्चारण के लिए शरीर के चार तंत्र:
1. नाभि-प्रदेश (मांसपेशी-बल तंत्र) – मांसपेशियाँ छाती को दबाती हैं।
2. छाती (वायु-बल तंत्र) – फेफड़ों से हवा ऊपर निकालती है।
3. गले का बॉक्स (ध्वनि तंत्र) – हवा गले के बॉक्स तक पहुँचती है।
4. मुँह (उच्चारण तंत्र) – हवा मुँह में प्रवेश कर मुँह/नाक में वर्ण रूप में प्रकट होती है।
मुँह के अंदर: मुँह (ओरल कैविटी), नाक (नेजल कैविटी)।
प्रक्रिया: नाभि-प्रदेश → छाती → गले का बॉक्स → मुँह → स्थानों में वर्ण उत्पत्ति।
३. वर्णोत्पत्त्यर्थं आवश्यकतत्त्वानि
त्रीणि तत्त्वानि:
स्थानं – वायुः यस्मिन् स्थले वर्णरूपेण प्रकटीभवति।
करणं – आस्यभागः स्थानं स्पृशति/समीपं याति।
आभ्यन्तरप्रयत्नः (अग्रे ज्ञास्यामः)।
हिन्दी अनुवाद
तीन तत्त्व:
स्थान – हवा जिस जगह वर्ण रूप में प्रकट होती है।
करण – मुँह का भाग स्थान को छूता/पास आता है।
आभ्यन्तर प्रयत्न (आगे जानेंगे)।
४. स्थानं (Place of Articulation)
आस्ये षट् स्थानानि:
मुखे: कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्तः, ओष्ठः (पञ्च)।
नासिकायां: नासिका (एकं)।
उदाहरणं: मुरलीं अङ्गुलिच्छिद्राणि स्थानानि इव।
हिन्दी अनुवाद
मुँह में छह स्थान:
मुँह में: कंठ, तालु, मूर्धा, दाँत, होंठ (पाँच)।
नाक में: नासिका (एक)।
उदाहरण: बाँसुरी के छेद स्थानों की तरह।
५. करणं (Tool of Articulation)
आस्यभागः स्थानं स्पृशति/समीपं याति।
तालु/मूर्धा/दन्तेषु: जिह्वा करणं।
तालव्येषु: जिह्वामध्यः।
मूर्धन्येषु: जिह्वोपाग्रः।
दन्त्येषु: जिह्वाग्रः।
कण्ठ/ओष्ठ/नासिकासु: स्वस्थानं करणं।
कण्ठ्येषु: कण्ठस्य अग्रभागः/पृष्ठभागः।
ओष्ठ्येषु: उत्तरोष्ठः/अधरोष्ठः।
नासिक्येषु: नासिकामूलस्य उपरिभागः/अधोभागः।
उदाहरणं: मुरलीं अङ्गुलयः करणानि इव।
हिन्दी अनुवाद
मुँह का भाग स्थान को छूता/पास आता है।
तालु/मूर्धा/दाँत में: जीभ करण है।
तालव्य में: जीभ का मध्य भाग।
मूर्धन्य में: जीभ का उपाग्र भाग।
दन्त्य में: जीभ का अग्र भाग।
कंठ/होंठ/नासिका में: स्वयं स्थान करण है।
कंठ्य में: कंठ का अग्र/पृष्ठ भाग।
ओष्ठ्य में: ऊपरी/निचला होंठ।
नासिक्य में: नासिका मूल का ऊपरी/निचला भाग।
उदाहरण: बाँसुरी में उँगलियाँ करणों की तरह।
६. शब्दार्थाः (Key Word Meanings)
नितान्तं: – अत्यन्तं (अत्यंत)
निर्दुष्टं: – दोषरहितं (दोषरहित)
नोदयन्ति: – अभिपीडयन्ति (दबाती हैं)
निःसारयति: – बहिः प्रेषयति (बाहर निकालती है)
सरन्: – चरन् (बढ़ना)
प्रकटीभवति: – उत्पद्यते (उत्पन्न होता है)
निदर्शने: – उदाहरणे (उदाहरण में)
मुरली: – वंशी (बाँसुरी)
परिभाषा: – शास्त्रीयव्याख्यानं (शास्त्रीय व्याख्या)
स्वरः – स्वयं राजन्ते (स्वयं राजन्ते)
व्यञ्जनं: – अन्वग् भवति (अन्वग् भवति)
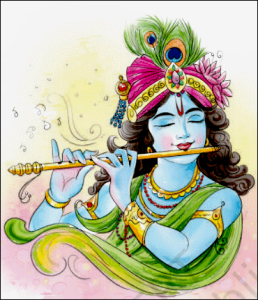
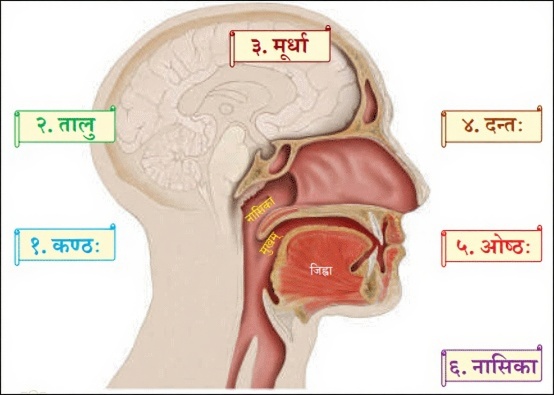
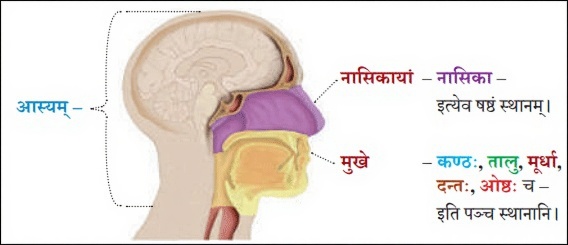
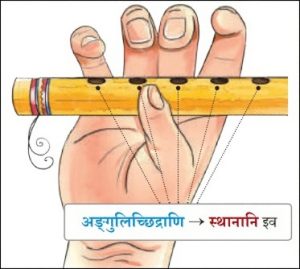
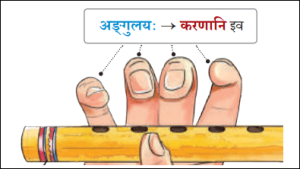

Leave a Reply