Notes For All Chapters – संस्कृत Class 7
हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः

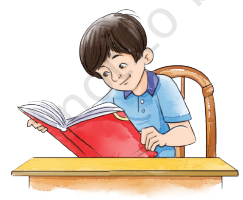

श्लोक 1
संस्कृत: माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः ॥
पदच्छेद: माता भूमिः, पुत्रः अहम्, पृथिव्याः।
अन्वय: भूमिः माता (अस्ति), अहं पृथिव्याः पुत्रः (अस्मि)।
भावार्थ (हिंदी):
पृथ्वी हमारी माता के समान हमारी रक्षा करती है और हमें पालती है। इसलिए पृथ्वी हम सभी की माता है। हम सभी इस पृथ्वी के सन्तान हैं और यह हमेशा पूजनीय है।
मुख्य विचार: पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र, जो सम्मान और श्रद्धा के पात्र हैं।
श्लोक 2
संस्कृत: न रत्नं अन्विष्यति, मृग्यते हि तत् ॥
पदच्छेद: न रत्नम्, अन्विष्यति, मृग्यते हि, तत्।
अन्वय: रत्नं न अन्विष्यति, तत् मृग्यते हि।
भावार्थ (हिंदी):
रत्न स्वयं खोजने नहीं जाते, बल्कि खोजने वाले ही रत्नों की खोज करते हैं। उसी तरह, यदि हममें गुण हैं, तो गुणों को पहचानने वाले स्वयं हमें खोज लेते हैं।
मुख्य विचार: मूल्यवान गुण बिना आत्म-प्रचार के पहचान आकर्षित करते हैं।
श्लोक 3
संस्कृत: शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ॥
पदच्छेद: शरीरम्, आद्यम्, खलु, धर्मसाधनम्।
अन्वय: शरीरं खलु आद्यं धर्मसाधनम्।
भावार्थ (हिंदी):
यदि हमारा शरीर स्वस्थ है, तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। इसलिए शरीर की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि यह धर्म के पालन का प्रथम साधन है।
मुख्य विचार: स्वस्थ शरीर कर्तव्यों और धर्म के पालन का प्राथमिक साधन है।
श्लोक 4
संस्कृत: क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् ॥
पदच्छेद: क्षणशः, कणशः, च, एव, विद्याम्, अर्थम्, च, साधयेत्।
अन्वय: क्षणशः (एव) विद्यां, कणशः एव अर्थं च साधयेत्।
भावार्थ (हिंदी):
ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय का निरंतर उपयोग करना चाहिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसी तरह, धन संग्रह करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति निरंतर छोटे-छोटे प्रयासों से धन इकट्ठा करे। ‘क्षण का त्याग करने से विद्या कहाँ, कण का त्याग करने से धन कहाँ।’
मुख्य विचार: समय और छोटे प्रयासों से विद्या और धन अर्जित किए जाते हैं।
श्लोक 5
संस्कृत: सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ॥
पदच्छेद: सुखार्थिनः, कुतः, विद्या, कुतः, विद्यार्थिनः, सुखम्।
अन्वय: सुखार्थिनः विद्या कुतः (भवेत्), विद्यार्थिनः सुखं कुतः (भवेत्)।
भावार्थ (हिंदी):
जो व्यक्ति सदा सुख की इच्छा रखता है, परिश्रम नहीं करता और आलसी है, वह विद्या कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे आलस्य और सुख का त्याग कर निरंतर विद्या अर्जन करना चाहिए।
मुख्य विचार: विद्या के लिए परिश्रम आवश्यक है, और विद्या अर्जन में सुख की तलाश नहीं की जाती।
श्लोक 6
संस्कृत: गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः ॥
पदच्छेद: गुणाः, पूजास्थानम्, गुणिषु, न च, लिङ्गम्, न च, वयः।
अन्वय: गुणिषु गुणाः (एव) पूजास्थानं (भवन्ति), लिङ्गं च न (भवति), वयः च न (भवति)।
भावार्थ (हिंदी):
गुणों का सदा सम्मान होता है। गुणी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, वह हमेशा पूजनीय होता है। सम्मान के लिए लिंग या आयु महत्वपूर्ण नहीं होती।
मुख्य विचार: गुण ही पूजनीय हैं, न कि लिंग या उम्र।
श्लोक 7
संस्कृत: मा ब्रूहि दीनं वचः ॥
पदच्छेद: मा, ब्रूहि, दीनम्, वचः।
अन्वय: (त्वं) दीनं वचः मा ब्रूहि।
भावार्थ (हिंदी):
समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ सहायता करते हैं, कुछ केवल शिकायत। इसलिए, स्वाभिमानी व्यक्ति को किसी के सामने सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए।
मुख्य विचार: स्वाभिमान के साथ दीन या याचना भरे शब्द नहीं बोलने चाहिए।
श्लोक 8
संस्कृत: यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् ॥
पदच्छेद: यः, तु, क्रियावान्, पुरुषः, सः, विद्वान्।
अन्वय: यः तु क्रियावान् पुरुषः, सः विद्वान् (भवति)।
भावार्थ (हिंदी):
जो व्यक्ति अपने ज्ञान को जीवन में आचरण, व्यवहार और प्रयोग द्वारा लागू करता है, वही वास्तव में विद्वान होता है, न कि केवल पढ़ने वाला। बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ है।
मुख्य विचार: ज्ञान का उपयोग करने वाला ही सच्चा विद्वान है।
श्लोक 9
संस्कृत: शीलं परं भूषणम् ॥
पदच्छेद: शीलम्, परम्, भूषणम्।
अन्वय: शीलं परं भूषणम् (अस्ति)।
भावार्थ (हिंदी):
मनुष्य का आचरण ही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। बिना अच्छे आचरण के अन्य गुण निरर्थक हैं।
मुख्य विचार: अच्छा चरित्र मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है।
श्लोक 10
संस्कृत: हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ॥
पदच्छेद: हितम्, मनोहारि, च, दुर्लभम्, वचः।
अन्वय: हितं मनोहारि च वचः दुर्लभं (भवति)।
भावार्थ (हिंदी):
कुछ लोग हितकारी बातें कहते हैं, परंतु कठोरता से। कुछ लोग मन को भाने वाली बातें कहते हैं, परंतु वे हितकारी नहीं होतीं। ऐसा वचन दुर्लभ है जो हितकारी भी हो और मनोरम भी।
मुख्य विचार: हितकारी और मधुर दोनों गुणों वाला वचन मिलना कठिन है।


Leave a Reply